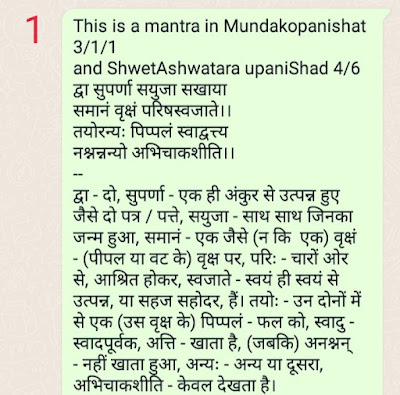एक-ध्रुवीय, द्वि-ध्रुवीय और त्रि-ध्रुवीय चेतना
-----------------------©----------------------
समस्त सांसारिक अनुभव तथा ज्ञान के अर्थ में चेतना सदैव एक द्वि-ध्रुवीय वास्तविकता है। जहाँ और जब भी चेतना का कार्य या गतिविधि किसी अनुभव, या ज्ञान के रूप में घटित होती है, तब वहाँ अपरिहार्यतः कोई न कोई विषय होता है और विषय तथा विषयी के मध्य का प्रसंग वृत्ति के रूप में पाया और देखा जाता है। विषय स्वयं जड होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यह संदेहास्पद है, जिसे न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही असिद्ध किया जा सकता है, - शायद यह प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। इसकी तुलना में जिस विषयी (चेतन) के प्रकाश में विषय (जड) वास्तविकता ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है, उसका अस्तित्व अकाट्यतः और निर्विवादतः स्वतंत्र है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चेतन (विषयी) और जड (विषय) एक ही चेतना के दो पक्ष हैं, क्योंकि अभी यह कहना जल्दबाजी ही होगा कि क्या किसी विषय के अभाव में चेतन (विषयी) का अस्तित्व संभव है! किन्तु यह तो कहा जा सकता है कि विषय (जड) और विषयी (चेतन) जिस चेतना में अस्त्तित्वमान होते हैं (या होते हुए प्रतीत होते हैं) वह आधारभूत अधिष्ठान / आधार नित्य, और सदैव एकरस विशुद्ध और अखंड वास्तविकता है। यद्यपि इस विवेचना में उसे 'वह' कहना भी त्रुटिपूर्ण है, किन्तु तात्कालिक और प्रयोजन की दृष्टि से इसका उपयोग है ही।
विषय-विषयी का संबंध ही मन है यही व्यक्तिगत अस्तित्व भी है क्योंकि मन सदैव और आवश्यक रूप से विषयी-केन्द्रित होता है । इस व्यक्तिगत विषयी का उल्लेख प्रत्येक मनुष्य "मैं" शब्द से करता है। इसकी तुलना में विषयमात्र का उल्लेख 'यह', 'वह' आदि शब्दों से किया जाता है। विषयी सदैव चेतन / 'मैं' है, और 'मैं' का उल्लेख 'यह' या 'वह' शब्द से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपने अस्तित्व को 'मैं' के रूप में जानना अनायास होता है, और यह जानना ही चेतना है। इसलिए जानना चेतना है, जबकि 'मैं' चेतन। जैसे ही 'मैं जानता हूँ' कहा जाता है, तो तुरन्त ही विरोधाभास पैदा होता है। इसलिए एक जानना वह है जिसमें जाननेवाला (ज्ञाता) और जाना हुआ (ज्ञेय) सत्य परस्पर अभिन्न होते हैं, जबकि एक जानना वह है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो भिन्न वस्तुएँ होती हैं। इस दूसरे प्रकार के जानने में ज्ञाता -जाननेवाला ही चेतन है, जबकि पहलेवाले जानने में ज्ञाता शुद्ध चेतना है।
फिर 'विचार' क्या है? क्या विषय और विषयी किसी एक या दोनों के अभाव में 'विचार' का अस्तित्व संभव है? 'विचार' पुनः शाब्दिक, भावनात्मक, स्मृति या कल्पना के रूप में हो सकता है। किन्तु है तो यह किसी न किसी स्थूल या सूक्ष्म विषय और चेतन के बीच होनेवाली कोई प्रक्रिया ही। इस वैचारिक प्रक्रिया के होते समय विषय और विषयी दूध और पानी की तरह एक दूसरे से मिले हुए से हो जाते हैं, और जैसे ही वैचारिक प्रक्रिया का विषय बदलता है, विषयी तत्क्षण ही किसी दूसरे विषय से एकात्म हो जाता है। फिर भी उसे भूल से भी इस बारे में कभी संशय तक नहीं होता कि उसका अस्तित्व सतत है। विभिन्न और विविध विषयों के विचार स्वरूपतः एक शाब्दिक, भावनात्मक या धारणात्मक अनुभव या स्मृति ही होते हैं, जिनके पुनः होने की कल्पना ही 'भविष्य' है। यही मन, समग्र मन, सामूहिक मन या सामूहिक चेतना है, इसलिए समस्त ज्ञान बीजरूप में सब में और प्रत्येक में ही विद्यमान होता है, और अपने व्यक्तिगत 'मैं' का विचार केवल वैचारिक भ्रम है।
चेतना इसलिए सार्वत्रिक, सार्वकालिक सत्य है, यद्यपि सर्वत्र (स्थान) काल (समय) भी चेतना की ही अभिव्यक्ति मात्र हैं।
***
शब्द-कुँजी (हिन्दी-अंगरेजी)
चेतना - consciousness
चेतन - sentient / conscious,
जड - insencient
शुद्ध चेतना - pure consciousness,
--