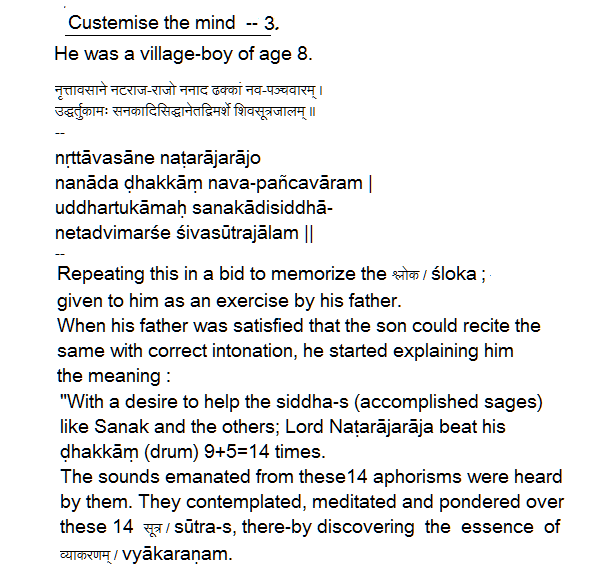चेतना और साक्षात्
--
अस् (होना) (अदादिगण - भू भवति - अस्ति है ।) :
'क्तिन्' प्रत्यय का ’ति’ शेष रहने से भाववाचक संज्ञा ’अस्तिः’ (exist) होता है ।
जन् (जन्म होना) :
'क्तिन्' प्रत्यय का ’ति’ शेष रहने से भाववाचक संज्ञा ’जातिः’ (being) होता है ।
इस प्रकार 'जो है' / अस्तित्व, वह ’भूत’ है, और जन्म ’जातिः’ होता है ।
इस प्रकार जीवमात्र तथा मनुष्य आदि भी जरायुज, उद्भिज्ज, अंडज, तथा स्वेदज इन चार जाति में से किसी में जन्म लेने से उस जाति का कहा जाता है ।
मनुष्य जाति में जन्म मात्र लेने से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण का या अवर्ण (वर्ण-व्यवस्था से इतर) नहीं हो जाता ।
जन्म से तो मनुष्यमात्र शूद्र ही होता है किन्तु संस्कार होने से वह सवर्ण होता है ।
यह संस्कार भी पूर्व-जन्म से प्राप्त हुआ भी और प्रसुप्त हो सकता है, अथवा अज्ञात कारणों से समय आने पर जागृत हो जाता है ।
यदि यह पहले से प्राप्त न हुआ हो, तो ग्रहण किया जा सकता है ।
भूतिः (exist होने) के बाद ही जातिः (being / जीव) है ।
जाति के बाद पुनः अनुभूति (feeling / experiencing) है ।
अनुभूति के बाद प्रतीति / भावना (emotion) है ।
प्रतीति होने के बाद मननशील प्राणियों अर्थात् मानव में भाषा का स्फुरण होता है ।
भाषा का तात्पर्य है ध्वनियों के संयोग से बने ’शब्द’ से किसी वस्तु का संबंध स्थापित करना ।
’मा’, ’पा’ ’ता’ ’दा’ आदि शब्द प्रायः माता-पिता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें शिशु बोलना तथा उनके अर्थ का साहचर्य स्थापित करना सीखता है ।
इस प्रकार धीरे-धीरे अनेक नए शब्द वह सीख लेता है जो वस्तुवाची (objective) तथा भाववाची (abstraction / abstract) अर्थ के द्योतक (indicative) होते हैं ।
अनुभूति (feeling / experiencing) सुखप्रद, दुःखप्रद या क्लिष्ट (मिली-जुली) हो सकती है ।
अनुभूति का दोहराव ’प्रतीति’ (emotion) का कारण है ।
’प्रतीति’ (emotion) तथ्य के अनुसार यथावत, या उससे भिन्न हो सकती है ।
भिन्न-भिन्न शब्दों को साथ साथ प्रयोग करने से ’विचार’ से इंगित की जानेवाली भाववाचक संज्ञा अस्तित्व में आती है । जिससे किसी वस्तु या वस्तु-विशेष का संकेत और बोध नहीं होता।
इसलिए ’विचार’ भाव-संप्रेषण में उपयोगी तो हो सकता है, उसके द्वारा प्रकट या ग्रहण किया जानेवाला भाव या तात्पर्य एक नितांत अमूर्त तत्व है ।
’विचार’ का परिणाम है स्मृति, -जो समस्त घटनाओं के मध्य एक सातत्य (क्रम) का सृजन करती है, और जो पुनः एक ’विचार’ ही होता है ।
इस प्रकार स्मृति से आच्छन्न चित्त अतीत की कल्पना करता है, और असंख्य घटनाओं को क्रम देते हुए उन्हें जोड़कर, केवल भ्रम और भूल से इस अतीत को एक ठोस सत्य समझा जाता है, जो वस्तुतः बस स्मृति का ही कमाल होता है।
इसी अतीत के परिप्रेक्ष्य में ’मैं’ नामक स्वसत्ता को आधारभूत केन्द्र समझ लिया जाता है, और यह समझ पुनः बुद्धि के अन्तर्गत ही संभव होती है ।
बुद्धि यद्यपि इस केन्द्र से स्वतन्त्र रहकर अपने नियमों से संचालित होती है तथापि बुद्धि पर अपना स्वामित्व अनुभव और प्रतीति जान पड़ता है ।
न तो अनुभव और न प्रतीति स्थिर / अटल होता है, जबकि वे जिसके अन्तर्गत और जिसके आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय होते रहते हैं वह तत्व ’चेतना’/ Consciousness सदा नेपथ्य में ही विद्यमान रहती है ।
जैसे विषय का प्रमाण विषयी की तरह विषय से भिन्न और अन्य होता है, चेतना स्वप्रमाणित और स्वयं सिद्ध होने से उसकी सत्ता का प्रमाण उस तरह उससे भिन्न और अन्य नहीं हो सकता ।
इस सत्य पर ध्यान / Attention / Awareness जाते ही उस चेतना को ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि जिस किसी प्रकार से शब्द देकर उसे व्यक्त किया जाता है ।
--
--
अस् (होना) (अदादिगण - भू भवति - अस्ति है ।) :
'क्तिन्' प्रत्यय का ’ति’ शेष रहने से भाववाचक संज्ञा ’अस्तिः’ (exist) होता है ।
जन् (जन्म होना) :
'क्तिन्' प्रत्यय का ’ति’ शेष रहने से भाववाचक संज्ञा ’जातिः’ (being) होता है ।
इस प्रकार 'जो है' / अस्तित्व, वह ’भूत’ है, और जन्म ’जातिः’ होता है ।
इस प्रकार जीवमात्र तथा मनुष्य आदि भी जरायुज, उद्भिज्ज, अंडज, तथा स्वेदज इन चार जाति में से किसी में जन्म लेने से उस जाति का कहा जाता है ।
मनुष्य जाति में जन्म मात्र लेने से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण का या अवर्ण (वर्ण-व्यवस्था से इतर) नहीं हो जाता ।
जन्म से तो मनुष्यमात्र शूद्र ही होता है किन्तु संस्कार होने से वह सवर्ण होता है ।
यह संस्कार भी पूर्व-जन्म से प्राप्त हुआ भी और प्रसुप्त हो सकता है, अथवा अज्ञात कारणों से समय आने पर जागृत हो जाता है ।
यदि यह पहले से प्राप्त न हुआ हो, तो ग्रहण किया जा सकता है ।
भूतिः (exist होने) के बाद ही जातिः (being / जीव) है ।
जाति के बाद पुनः अनुभूति (feeling / experiencing) है ।
अनुभूति के बाद प्रतीति / भावना (emotion) है ।
प्रतीति होने के बाद मननशील प्राणियों अर्थात् मानव में भाषा का स्फुरण होता है ।
भाषा का तात्पर्य है ध्वनियों के संयोग से बने ’शब्द’ से किसी वस्तु का संबंध स्थापित करना ।
’मा’, ’पा’ ’ता’ ’दा’ आदि शब्द प्रायः माता-पिता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें शिशु बोलना तथा उनके अर्थ का साहचर्य स्थापित करना सीखता है ।
इस प्रकार धीरे-धीरे अनेक नए शब्द वह सीख लेता है जो वस्तुवाची (objective) तथा भाववाची (abstraction / abstract) अर्थ के द्योतक (indicative) होते हैं ।
अनुभूति (feeling / experiencing) सुखप्रद, दुःखप्रद या क्लिष्ट (मिली-जुली) हो सकती है ।
अनुभूति का दोहराव ’प्रतीति’ (emotion) का कारण है ।
’प्रतीति’ (emotion) तथ्य के अनुसार यथावत, या उससे भिन्न हो सकती है ।
भिन्न-भिन्न शब्दों को साथ साथ प्रयोग करने से ’विचार’ से इंगित की जानेवाली भाववाचक संज्ञा अस्तित्व में आती है । जिससे किसी वस्तु या वस्तु-विशेष का संकेत और बोध नहीं होता।
इसलिए ’विचार’ भाव-संप्रेषण में उपयोगी तो हो सकता है, उसके द्वारा प्रकट या ग्रहण किया जानेवाला भाव या तात्पर्य एक नितांत अमूर्त तत्व है ।
’विचार’ का परिणाम है स्मृति, -जो समस्त घटनाओं के मध्य एक सातत्य (क्रम) का सृजन करती है, और जो पुनः एक ’विचार’ ही होता है ।
इस प्रकार स्मृति से आच्छन्न चित्त अतीत की कल्पना करता है, और असंख्य घटनाओं को क्रम देते हुए उन्हें जोड़कर, केवल भ्रम और भूल से इस अतीत को एक ठोस सत्य समझा जाता है, जो वस्तुतः बस स्मृति का ही कमाल होता है।
इसी अतीत के परिप्रेक्ष्य में ’मैं’ नामक स्वसत्ता को आधारभूत केन्द्र समझ लिया जाता है, और यह समझ पुनः बुद्धि के अन्तर्गत ही संभव होती है ।
बुद्धि यद्यपि इस केन्द्र से स्वतन्त्र रहकर अपने नियमों से संचालित होती है तथापि बुद्धि पर अपना स्वामित्व अनुभव और प्रतीति जान पड़ता है ।
न तो अनुभव और न प्रतीति स्थिर / अटल होता है, जबकि वे जिसके अन्तर्गत और जिसके आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय होते रहते हैं वह तत्व ’चेतना’/ Consciousness सदा नेपथ्य में ही विद्यमान रहती है ।
जैसे विषय का प्रमाण विषयी की तरह विषय से भिन्न और अन्य होता है, चेतना स्वप्रमाणित और स्वयं सिद्ध होने से उसकी सत्ता का प्रमाण उस तरह उससे भिन्न और अन्य नहीं हो सकता ।
इस सत्य पर ध्यान / Attention / Awareness जाते ही उस चेतना को ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि जिस किसी प्रकार से शब्द देकर उसे व्यक्त किया जाता है ।
--